
सुशोभित
एक से ज़्यादा वजहें थीं कि उज्जैन में तोपख़ाने से लेकर मदार गेट तक के इलाक़े का चप्पा-चप्पा मैंने छान रक्खा था।


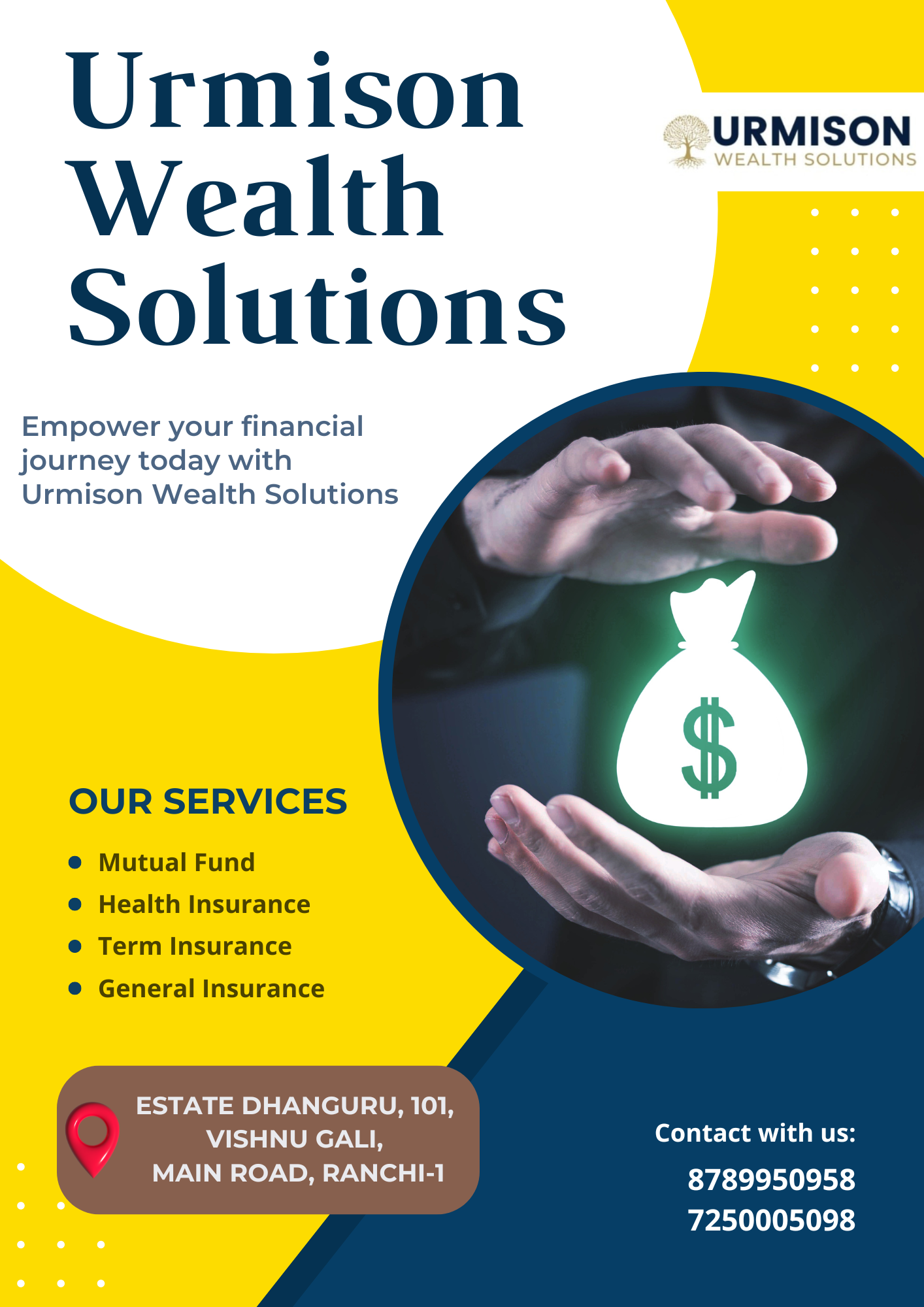
अव्वल तो यही कि मुझको उर्दू का क़ाएदा सिखाने वाले जनाब शम्स-उल-हसन क़ादरी साहब का हालमुकाम मदार गेट में काँच मंदिर के पीछे मिर्ची सेठ वाली गली में था। दूसरे ये कि जिस पेपर की बंदी मैं बाँटता था, उसका छापाख़ाना वहीं नज़दीक़ दौलतगंज, घी-मंडी में ही था। तीसरे ये कि मगरमुँहा- जहाँ मेरा घर था- से दौलतगंज जाने का सबसे सीधा रास्ता पानदरीबा, गुदरी, लोहे का पुल होकर मदार गेट ही था।
ये लोहे का पुल तो अब वहाँ नहीं है, लेकिन एक ज़माने में वहाँ एक नाला हुआ करता था, जिस पर ख़ालिस फ़ौलाद का वह बंधान था। वहीं पर घोड़ी वालों की गली थी, जहाँ से शादी-ब्याह के लिए घोड़ियाँ किराये पर ली जातीं। इस जादुई गली में सजी-धजी हसीन घोड़ियाँ इतराती बलखाती रहतीं। बग्घियाँ सजी रहतीं। घुंघरू खनकते रहते। लीद महकती रहती!
ये भी एक इत्तेफ़ाक़ ही था कि मेरे पेपर की बहुतेरी बंदियाँ मदार गेट की थीं। वहाँ मैं गुलरेज़ बेकरी में पेपर डालता था, बादशाही होटल में डालता था, क़ुरैशी एग्ज़ सेंटर में डालता था, और बड़ी फ़ज़र बाबू ख़ाँ साइकिल-पंक्चर वाले के यहाँ सुबह का अख़बार डालने का ज़िम्मा भी मेरा ही था।
ये बाबू ख़ाँ निहायत ही नेक और शरीफ़ आदमी थे। धूप में झुलसे उनके साँवले चेहरे पर मुस्कराहट हमेशा सजी रहती। उन पर बारीक़ कतरी मूँछें फबतीं, जिनमें जहाँ-तहाँ सफ़ेदी बरामद होने लगी थी। उनकी दुकान पर साइकिलें दुरुस्त की जातीं और किराये पर भी दी जातीं। एटलस की साइकिलें उनकी दुकान के बाहर घोड़ियों जैसी ही धज से खड़ी रहतीं, जिनकी रिम को वे बहुत प्यार से कपड़ा मारकर चमकाते। दुकान का फ़र्श ग्रीज़ और ऑइल से काला पड़ गया था। एक बोझल गंध उसमें हमेशा टंगी रहती। दीवारें बदरंग हो चली थीं। नीला रंग पुते लोहे के शोकेस पर चलताऊ शायरियाँ लिखी थीं। पेण्डुलम वाली एक घड़ी उस दुकान में मुझको देखकर हमेशा हाथ हिलाती रहती।
मैंने बाबू ख़ाँ के हाथ कभी साफ़ नहीं देखे थे। वे दिन भर पंक्चर पकाते और उनके हाथों पर, अंगुलियों पर, नाख़ूनों के भीतर कालिमा बसी रहती। वो ख़ाकी रंग की कमीज़ पहनते थे और वो भी हमेशा दाग़दार रहती। मैं बाबू भाई के यहाँ ही अपनी साइकिल का पंक्चर पकवाता था। कारण, उनके यहाँ मैं पेपर डालता था और पंक्चर पकाने के पैसे मुझको जेब से नहीं देना पड़ते थे। ग़रज़ ये कि मगरमुँहा से मदार गेट तक साइकिल घसीटकर ले जाना मुझको मंज़ूर था, लेकिन बाबू भाई के होते किसी और को पंक्चर पकाने के तीन रुपए देना मंज़ूर नहीं था। बाबू भाई ये बात जानते थे। वो हमेशा ख़ुश मन से पंक्चर पकाते। फिर मुस्कराकर मेरी तरफ़ देखते मानों पूछ रहे हों, पंक्चर का पैसा? मैं कहता, पेपर के बिल से काट लेना। वो कहते, दुरुस्त बात मियाँ। और बताओ, क्या ख़िदमत करूँ? चाय पिलाऊँ? हम कहते, हाँ पिलाओ। वो मदीना होटल से मुसलमानी चाय बुलवाते, जिसमें चुटकी भर नमक पड़ता। जिस दिन तरंग में होते, उस दिन बेमिसाल बेकरी का टोस्ट भी खिलाते।
एक बार भी तब मेरे ज़ेहन में ये ख़याल नहीं आता था कि अगर पंक्चर का पैसा पेपर के बिल से काटा जा सकता था तो चाय का पैसा पेपर के बिल में क्यों नहीं जोड़ा जा सकता था? ना ही उन्होंने कभी माँगा। ये असूल वाली बात थी। पेपर डालना मेरा काम था, पंक्चर पकाना उनका काम था। काम की काट काम से होती थी। चाय पिलाना, सुपारी खिलाना तो मेहमाननवाज़ी के हिस्से में आता था। उसका कोई पैसा-वैसा नहीं लगता।
मैं बाबू ख़ाँ के पंक्चर पकाने के हुनर पर फ़िदा था। वो बहोत शाइस्ता तरीक़े से इस काम को अंजाम देते। बड़ी नज़ाक़त से साइकिल का पहिया खोलते, रिम से ट्यूब को उचकाकर बाहर निकालते, फिर हाथ से चलाए जाने वाले एयर-पम्प से उसमें हवा डालते। हवा डालते समय उनके कूल्हे मटकने लगते। मैं हँसी दबा लेता। पानी की बाल्टी में ट्यूब डुबोकर वे पंक्चर की शिनाख़्त करते। फिर किसी फटे हुए ट्यूब से टिकिया काटते। मुझको लगता टिकिया काटने में उनको ख़ास मज़ा आता था, जैसे वो पंक्चर की टिकिया नहीं, किसी सितारे-हिन्द की सजावट का सामान हो! पीतल की धारदार कैंची से वो टिकिया को देर तक सजाते-सँवारते, गोल-गोल उसको काटते, जैसे कि इस हुनरमंदी का कोई ईनाम उनको मिलेगा। फिर उस टिकिया पर सॉल्यूशन लगाते, दियासलाई जलाकर उसको आग दिखाते, उसी तीली से बीड़ी जलाते। मुँह में बीड़ी दबाए टिकिया चिपकाते, ठोंक-बजाकर बराबर करते, ट्यूब को टायर में फँसाते, उसमें फिर हवा भरते, वॉल्व पर थूक लगाकर जाँचते कि कहीं हवा तो नहीं निकल रही। सब तरफ़ से मुतमईन होने के बाद साइकिल स्टैंड पर खड़ी कर देते- लो मियाँ, तुम्हारी शाही सवारी तैयार!
बात-बेबात पर शुक्रिया कहने की उस ज़माने में रवायत नहीं थी तो मैं नहीं ही कहता। शुक्रिया कहने जैसा था भी क्या। बाबू भाई का काम ही था पंक्चर पकाना। मैं साइकिल उठाकर चल देता। ये हर हफ्ते-पखवाड़े की बात थी, इसमें नया कुछ नहीं था।
एक दिन मेरे घर पर बाबू ख़ाँ के घर से दावत का न्योता आया। मालूम हुआ, उनकी साली साहिबा का ब्याह था। वलीमे की दावत घर पर ही रखी थी। नलिया बाखल में उनका ठिकाना था। दावत का कार्ड मिलने तक मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि बाबू भाई का भी कोई घर हो सकता था। मुझको लगता था वो रात को उस बदरंग दीवार वाली दुकान में ही चटाई बिछाकर सो जाते होंगे। उन्होंने दावत के लिए मुझे याद रखा, इस बात से ख़ुश हुआ। पता पूछते उनके घर पहुँचा। गुलाब की लड़ियों से सजे दरवाज़े से भीतर घुसा। बरामदे में दुल्हन का दीदार किया। एक अंदरून अहाते में दावत के लिए बैठे। बड़े-से थाल में- जैसे कि मुसलमानी रिवाज़ होता है- रूमाली रोटियाँ, पुलाव, समोसे, पापड़, इमरतियाँ और सब्ज़ी-तरकारी पेश की गई।
लेकिन मेरी नज़र बाबू भाई को ढूँढ़ती रही। क्या बात है, वो नज़र क्यों नहीं आ रहे? बड़ी देर के बाद हुज़ूर नमूदार हुए। सुनहरी जरी वाली शानदार शेरवानी में! ये क्या बाबू ख़ाँ पंक्चर वाले ही हैं? इनके कपड़े आज इतने उजले और शफ़्फ़ाक़ कैसे? वो हमको देखकर मुस्कराए, हाथ मिलाया। अचरज कि इस हाथ पर आज कालिख के दाग़ नहीं थे। मैंने उनकी हथेलियों की गर्माहट महसूस की। वो हाथ निहायत ही मुलायम था। मैंने तो सोचा था कि पंक्चर पकाने वाले का हाथ खरोंचों से भरा और सख़्त होना चाहिए था। और ये नगीने वाली अंगूठी बाबू भाई ने किस सिंगार-पेटी में छुपाकर रखी थी? ये तो मैंने पहले कभी उनकी अंगुली में नहीं देखी थी। जूतियाँ तो देखो, कैसी चमचमाती-चोंचीली हैं। चलने पर चरमराती हैं। ख़ालिस चमरौंधा! और केवड़े और गुलाबख़ास के इत्र की ये मिली-जुली महक कैसी। आज उनके बदन से ग्रीज़ की बू क्यों नहीं आ रही?
उस दिन से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि बाबू ख़ाँ का उस साइकिल की दुकान के बाहर भी कोई वजूद हो सकता था। उसी दिन मुझको ये मालूम हुआ कि एक आदमी का जो चेहरा सालोंसाल आपको दिखता रहे, ज़रूरी नहीं कि उसकी जेब में रखा वो इकलौता चेहरा हो। उसके पास अपने बारे में सुनाने के लिए दूसरे अफ़साने भी हो सकते हैं।
यह साल गून्नीस सौ छन्नू का वाक़िया है। उसको बीते आज अठाइस साल हो रहे। मदार गेट की गलियाँ तो क्या, उज्जैन शहर ही छूटे अरसा हुआ। कुछ साल पहले एक पारिवारिक समारोह में उज्जैन जाना हुआ। दौलतगंज की ओर ही कार्यक्रम था। तो मैं तोपख़ाने वाले अपने जाने-पहचाने रास्ते पर चला आया। लेकिन वहाँ तो पूरी तस्वीर ही बदली हुई थी। लोहे के पुल से देवासगेट तक की पूरी सड़क हुकूमत ने चौड़ी कर दी थी, पतली गली से शाहराह बना दिया था। अंदाज़े मुताबिक़ उस जगह जाकर खड़ा हुआ, जहाँ बाबू भाई की साइकिल की दुकान किसी ज़माने में हुआ करती थी, लेकिन अभी तो वहाँ उसका नामो-निशान नहीं। कूल्हे मटकाकर साइकिल के पहिये में हवा भरने वाले बाबू ख़ाँ पंक्चर वाले हवा की मीनार की तरह ही कहीं गुम हो गए थे। कितनी आसानी से आज हम किसी को पंक्चर वाला बोलकर उसको नीचा दिखा देते हैं? बुनकरों, कारीगरों, जुलाहों को आँख उठाकर नहीं देखते। होम डिलीवरी करने वाले, कबाड़ी वाले से सरोकार नहीं रखते। चूड़ियाँ बेचने वालों के वजूद को देखकर अनदेखा कर देते हैं। बड़े-बड़े काम करने वाले दुनिया बनाते हैं, लेकिन दुनिया को छोटे-छोटे काम करने वाले ही चलाते हैं। बाबू ख़ाँ पंक्चर वाले जैसी अनगिन कहानियाँ उनके भीतर छुपी होती हैं।

