
सुशोभित
राहुल गांधी आज कोई पंद्रह सालों से सार्वजनिक जीवन में हैं और इतना समय किसी आदमी की परख करने के लिए बहुत होता है। राहुल में जो भोलापन और भलापन, ईमानदारी और सच्चाई है, उसे अनेक मित्र उनका बौड़म होना भी बतला सकते हैं।


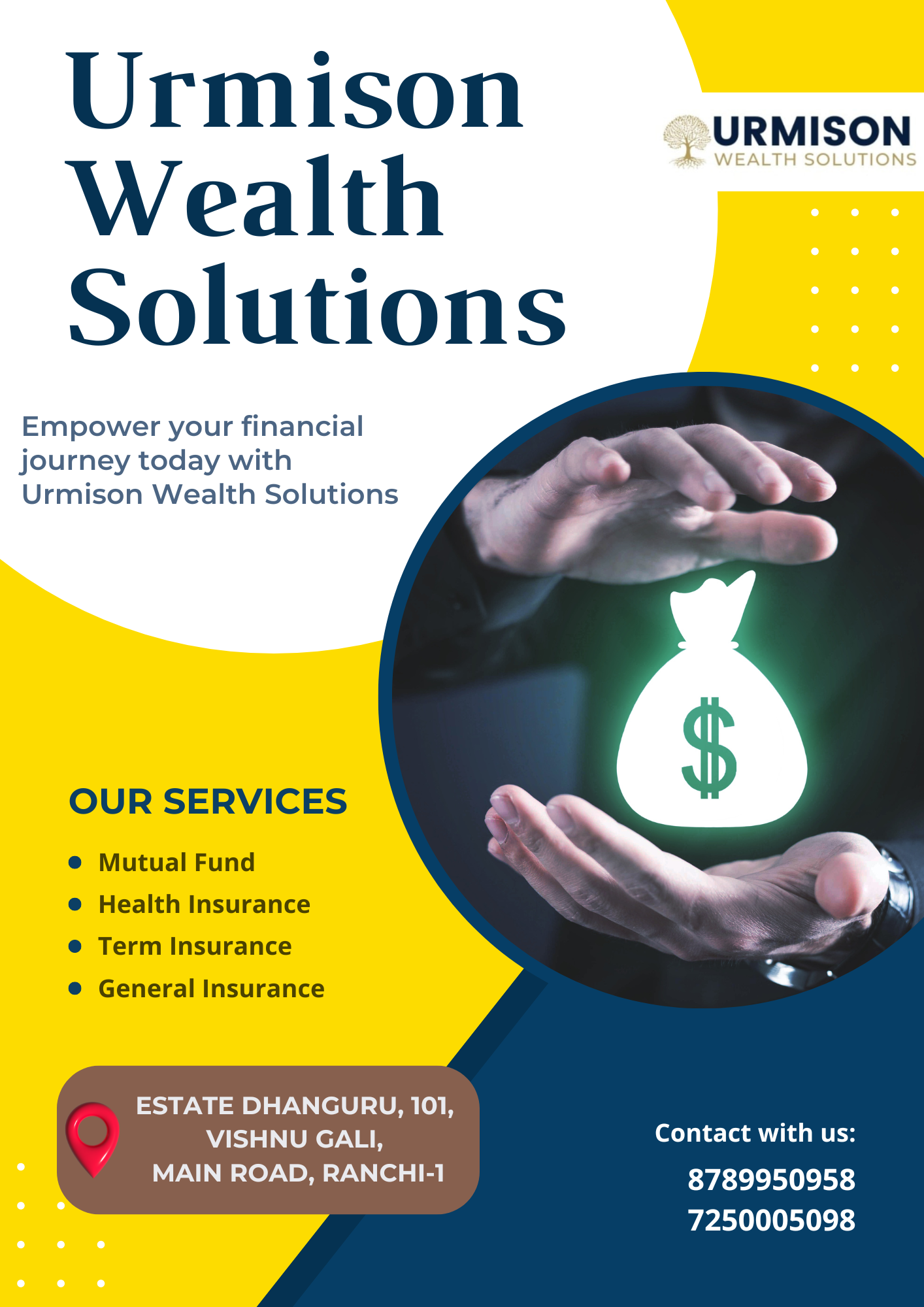
तिस पर मैं कहूँगा कि बौड़म होना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ इससे आप एक अच्छे राजनेता भले नहीं माने जाएँ, लेकिन राजनीति जीवन का एक आयाम भर है, पूरा जीवन नहीं है।
और राजनीति में विफल होने का मतलब जीवन में विफल होना नहीं है। इसका उलटा भी सही है। कोई राजनीति में बड़ा सफल होकर भी मनुष्य के रूप में विफल रह सकता है। उदाहरणों की हमारे यहाँ कमी नहीं।
राहुल का मामला ज़रा अजीब है। भला कौन राजनेता सार्वजनिक रूप से सत्ता को ‘ज़हर’ बताकर उसके प्रति अरुचि जतलाता है? उनकी माँ ने 2004 में प्रधानमंत्री बनने के अवसर को त्याग दिया था और बहुत सम्भव है कि राहुल भी वैसा अवसर बनने पर यही करें। यह अन्यमनस्कता राहुल के व्यक्तित्व का केंद्रीय हिस्सा बन चुकी है। क्या वे सच में ही राजनेता बनना चाहते थे? क्या कोई दूसरा कॅरियर उनके लिए बेहतर हो सकता था? ये प्रश्न असंख्य बार पूछे जा चुके हैं। किन्तु इतनी हार, उपहास और अपमान के बावजूद राहुल अभी तक भागे नहीं हैं, उलटे पहले से ज़्यादा ज़िद्दी होकर मैदान में डट गए हैं। ऐसा भी नहीं है कि राजनीति में भलमनसाहत हमेशा ही एक अयोग्यता साबित हो। जनता के मन का क्या भरोसा? जनता ने अगर चतुरसुजानों और धूर्तों और कुटिलों से ऊबकर मन बदलने का निर्णय कर लिया तो?
नेशनल हेरल्ड मामले में जब राहुल से कई दिनों तक घंटों पूछताछ चल रही थी तो उसके बाद एक सभा में किसी ने पूछा कि राहुलजी आपने इतने धीरज से इस सबका सामना कैसे किया? उन्होंने कहा, भैया मैं कांग्रेस में काम करता हूँ, धीरज तो आ ही जाएगा। मुझे याद नहीं आता मैंने कब आख़िरी बार किसी राजनेता के मुँह से ऐसी ईमानदार स्वीकारोक्ति, स्वयं पर किया गया ऐसा कटाक्ष और वह भी किसी आत्मदया के बिना सुना था। मैं इस बात की इज़्ज़त करता हूँ। यह कैंडिड-मोमेंट एक्नॉलेजमेंट का हक़दार है। और राहुल के व्यक्तित्व में ऐसे कैंडिड-मोमेंट्स भरे पड़े हैं।
एक नाकाम नेता कहकर राहुल का कोई भले जितना मखौल उड़ा ले, एक व्यक्ति होने की अस्मिता उनसे कोई नहीं छीन सकता। प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति में निहित ईमानदारी, सच्चाई और भोलेपन का कोई महत्व है या नहीं, या हम इन मूल्यों को घोलकर पी गए हैं? वैसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि राहुल गांधी बीते डेढ़ दशक से कठोर उपहास सह रहे हैं, किन्तु अभी तक कटु या उग्र या कुंठित नहीं हुए हैं। यह सरल बात नहीं है। इतनी पराजय, इतनी निराशा और इतने कटाक्ष सुनकर कोई भी कुंठित हो सकता था। शायद यह भी सच हो कि देश का शिक्षित वर्ग मन ही मन राहुल को पसंद करता है, अलबत्ता उनको वोट देने के प्रश्न पर उसके मन में दुविधा हो। क्योंकि देश चलाना एक बात है, भला आदमी होना दूसरी बात है। आज हम मान चुके हैं कि राज-काज के लिए टेढ़ा आदमी होना ज़रूरी है। लोगों ने मान लिया है कि लोहा ही लोहे को काटता है और घी टेढ़ी उंगली से ही निकलता है। यही मान्यता सख़्त प्रशासक को चुनवाती है, जो साम-दाम-दण्ड-भेद से काम निकलवाना जानता हो। लेकिन कब तक? कभी तो जनता टेढ़ेपन से तंग आकर सीधेपन की ओर आकृष्ट होगी? लोग तो मीठे से भी ऊब जाते हैं, कड़वे को कब तक झेलेंगे?
क्या ही अचरज है कि जिस व्यक्ति को ‘शहज़ादा’ कहकर पुकारा गया था और जो वंशवादी राजनीति का प्रतीक बना दिया गया था, वह सड़कों पर उतरकर लोगों से उनकी तुलना में ज़्यादा घुलता-मिलता है, जिन्हें जनप्रिय नेता बताया जाता है। 1951 में नेहरूजी भी इसी तरह से सड़कों पर उतरे थे और पूरे देश की परिक्रमा की थी। वह उनकी ‘भारत की दूसरी खोज’ थी। जबकि आज देश के बाहुबली नेता लोगों से फ़ासले से मिलते हैं। आभासी छवियों से उनको समझते हैं। उनमें गौरव या उन्माद की भावनाएँ जगाते हैं, मानो एक नागरिक का इसके सिवा और कोई काम नहीं रह गया है कि अहर्निश किसी न किसी बात पर गर्व करता रहे। कुछ नेता तो पत्रकारों का सामना करने से भी डरते हैं। जबकि राहुल तमाम प्रश्नों का सामना करते हैं और यह जानकर करते हैं कि शायद वे धरे जाएँ। क्योंकि प्रश्न टेढ़े होते हैं और राहुल अकसर दुविधा में पड़ जाते हैं या कोई अटपटी बात बोल जाते हैं। प्रतिपक्ष के मुस्तैद कैमरे उस क्षण को दबोच लेते हैं और पूरे देश को दिखाते फिरते हैं कि देखिये, यह व्यक्ति कितना मूर्ख है। हो सकता है कि हो, पर वह प्रश्नों का सामना तो कर रहा है। उनसे भाग तो नहीं रहा। क्या इस बात का कोई मूल्य नहीं है?
वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग ने हाल ही में एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि राहुल चाहकर भी सत्तापक्ष पर उसके स्तर तक जाकर प्रहार नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उनका संस्कार वैसा नहीं है। राहुल का संस्कार कांग्रेस पार्टी के उस संस्कार से जुड़ा है, जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। जबकि सत्तारूढ़ दल का संस्कार- और याद रहे यहाँ पर दीनदयाल-श्यामाप्रसाद, अटल-आडवाणी की नहीं वर्तमान के सत्तातंत्र की बात की जा रही है- गोधरा से उत्पन्न हुआ है। उसे परस्पर संघर्ष, ध्रुवीकरण और उपद्रव में ही अपना अंतिम मोक्ष दिखलाई देता है। जहाज़ के पंछी की तरह वह बार-बार साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण पर लौट आता है। जबकि राहुल गांधी ‘मोहब्बत की दुकान’ की बात करते हैं और वो इतने मासूम हैं कि 2019 में जब वो चुनाव हारे तो पत्रकार-वार्ता में उन्होंने कह दिया कि “प्यार कभी नहीं हारता है, प्यार कभी नहीं हार सकता है।” यह राजनीति की भाषा नहीं है। पर यह राजनीति की भाषा क्यों नहीं हो सकती? भले, सुशिक्षित, सौम्य लोगों को देश चलाने के योग्य नहीं समझा जाए- क्या यह एक अच्छी बात है?
आश्चर्य यह भी है कि भारतीय राजनीति के प्रथम परिवार से होने के बावजूद राहुल का व्यक्तित्व समाजवादी साँचे में ढला है और उनके गुण राजनेता से ज़्यादा कार्यकर्ताओं वाले हैं। महात्मा गांधी कांग्रेस के लीडरान से कहते थे कि हमें प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री बनने से ज़्यादा जनता के बीच जाकर काम करने की चिंता करनी चाहिए, जनता पर हमारा प्रभाव, उससे हमारा जीवंत सम्पर्क होगा तो हम चाहे जिसको प्रधानमंत्री बना देंगे। लेकिन जनता से ही अगर कट गए तो आज नहीं तो कल, कुर्सी भी जायेगी। राहुल वैसी ही जनोन्मुख राजनीति करते प्रतीत होते हैं। लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और राहुल फिर से अपने घोषणा-पत्र के साथ मैदान में हैं। उनकी भाषा-शैली, सोच-समझ, आचार-विचार-संस्कार की तुलना दूसरी पार्टी के नेताओं से की जा सकती है। और अगर मतदाता दोनों का आकलन करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचें कि राहुल को एक बार पाँच साल के लिए देश की कमान सौंपकर देखनी चाहिए, तो इसके लिए उन्हें दोष नहीं दिया जा सकेगा!

